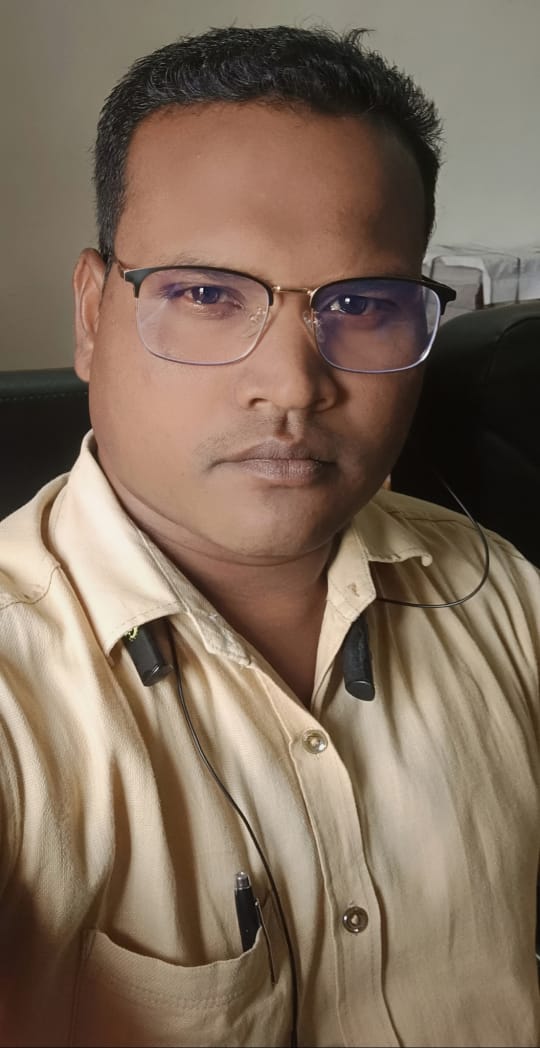लेखक/विचारक: महेन्द्र सिंह मरपच्ची
जब हम “विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस” मनाए है, 28 जुलाई को तो क्या हमे इस अवसर पर केवल प्रतीकात्मक पौधरोपण करना था नहीं बल्कि आत्मचिंतन और पृथ्वी की पीड़ा को समझने के लिए भी जरूरी था । इस आधुनिक सभ्यता की दौड़ में हमने जिन पहाड़ों को काटा है, जिन नदियों को मोड़ा है, जिन जंगलों को जला दिया है और जिन पशु-पक्षियों की चीत्कारों को अनसुना कर दिया है, वे सभी अब लौटकर हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के इस दौर में हमने विकास का अर्थ केवल खनन, निर्माण और मुनाफे में समेट दिया है, लेकिन इस मुनाफे की बुनियाद प्रकृति के विनाश पर टिकी हुई है। इसी संदर्भ में यदि कोई समुदाय है जिसने बिना लिखित संविधान के पहले हजारों वर्ष पूर्व प्रकृति के साथ सहजीवन स्थापित किया है, तो वह है कोयतुर समुदाय अर्थात सभी ट्राइबल जनजाति है। कोयतुर समुदाय की जीवनदर्शन केवल एक कोयतुरीयन परंपरा नहीं, बल्कि वह गहरी जीवनशैली है जो मानव और प्रकृति को एकात्म मानती है। कोयतुरों के लिए पेड़ केवल लकड़ी नहीं, देवता हैं, जंगल केवल संसाधन नहीं, पवित्र गृह हैं, और नदी केवल पानी नहीं, जीवित देवी हैं। उनका यह संबंध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि परंपराओं, त्योहारों, नियमों और सामुदायिक अनुशासन से पक्का बंधा हुआ है। उनके गीतों में वृक्ष गाते हैं, उनके नृत्यों में पर्वत थिरकते हैं, और उनकी कहावतों में जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई की चेतावनी मिलती है। वे ‘देव से पहले वन’ की धारणा में विश्वास रखते हैं और हर प्राकृतिक तत्व को पेन शक्ति के रूप में पूजते हैं। कोयतुरों के जंगलों में प्रवेश करते समय वे अपने पेन देवताओं से अनुमति मांगते हैं, शिकार या कटाई से पहले क्षमा याचना करते हैं, और जो कुछ लेते हैं उसका बदला देना जरूरी मानते हैं। यह परंपरा केवल संस्कृति नहीं, बल्कि वह जीवनशैली है जो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में सहायक रही है। कोयतुर जीवनशैली टिकाऊ ही नहीं बल्कि विकास का आदर्श मॉडल भी है
कोयतुर जीवनशैली टिकाऊ ही नहीं बल्कि विकास का आदर्श मॉडल भी है
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के हजारों गांवों में फैली यह कोयतुर सभ्यता आज भी टिकाऊ जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, कोरबा, सरगªुजा, जशपुर जैसे जिलों में बसे कोयतुर समुदायों की जीविका लघु वनोपज, पारंपरिक खेती और वर्षा जल पर आधारित जीवन प्रणाली से चलती है। वे पेड़ की जड़ नहीं काटते, केवल फल और पत्तों का उपयोग करते हैं। वे जंगल को सामूहिक संपत्ति मानते हैं और प्रत्येक निर्णय ग्रामसभा में लेते हैं। कोयतुर समुदाय की गोटुल प्रणाली एक ऐसी सामाजिक पाठशाला है जहां बच्चे प्रकृति से जुड़ना, सामूहिकता, नैतिकता और धरती के साथ संवाद करना सीखते हैं। यह जीवनदर्शन आधुनिक शिक्षा और विकास के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है जो हमें टिकाऊ भविष्य की ओर लेकर जाता है।
खनन और पूंजीपति की राजनीति ने निगल लिए छत्तीसगढ़ की लाखों हेक्टेयर जंगल
वहीं दूसरी ओर यदि हम तथाकथित मुख्यधारा विकास की ओर देखें तो भारत ने 2001 से 2024 तक लगभग 24.33 लाख हेक्टेयर जंगलों को उखाड़ कर फेक दिया है। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जहां 41 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है, यहां लगभग 2.31 लाख हेक्टेयर वृक्ष आवरण नष्ट हो चुका है। आकड़ो की माने तो कोरबा में 18,200 हेक्टेयर, सरगुजा में 13,300, रायगढ़ में 9,870, जशपुर में 8,500, बलरामपुर में 7,300, बस्तर और दंतेवाड़ा मिलाकर लगभग 19,000 हेक्टेयर वन समाप्त हो चुका हैं। यह सब अधिकतर कोयला खनन, बाँध निर्माण, औद्योगिक कॉरिडोर और सड़क परियोजनाओं के कारण हुआ है। इन विनाशों के पीछे अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों की परियोजनाएं रही हैं जिन्हें सरकारों ने खुलेआम अनुमति दी है, वह भी तब जब ग्रामसभा ने विरोध में प्रस्ताव पारित किए थे। विशेष रूप से हसदेव अरण्य क्षेत्र में ग्रामसभाएं बार-बार कहती रहीं कि हम कोयला खनन नहीं चाहते है लेकिन राज्य सरकारों ने या तो फर्जी ग्रामसभाएं आयोजित कीं या ग्रामवासियों को धोखा देकर मंजूरी प्राप्त कर ली

संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी के साथ पांचवीं अनुसूची, पेसा और वन अधिकार कानून का खुलेआम हो रहा है उपेक्षा
यह न केवल संविधान की आत्मा के खिलाफ है बल्कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची का सीधा उल्लंघन है। संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाई गई है जिसमें राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी सामान्य कानून को संशोधित हाने से रोके या बदल सके यदि वह जनजातीय हित में न हो। अनुच्छेद 244(1) स्पष्ट करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विशेष कानून लागू होते हैं। अनुच्छेद 275 केंद्र को यह निर्देश देता है कि वह इन क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक सहायता दे, लेकिन व्यावहारिक रूप में यह सहायता खनन परियोजनाओं में ही जाती है। पांचवीं अनुसूची की धारा 4 के अनुसार, राज्यपाल को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सलाह लेनी होती है, किंतु अधिकांश मामलों में यह केवल औपचारिकता बन गई है।

पेसा अधिनियम 1996 (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) संविधान के अनुच्छेद 243-M के तहत लाया गया था ताकि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को विशेष अधिकार मिल सकें। पेसा की धारा 4 (K) कहती है कि खनन, भूमि अधिग्रहण या अन्य परियोजनाओं में ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य होगी। धारा 4(I) के अनुसार ग्रामसभा के अनुमति बिना भूमि नहीं ली जा सकती। धारा 4(M) वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार ग्रामसभा को देती है। लेकिन वास्तविकता में यह सब झूठ साबित हुआ जब हसदेव अरण्य में दो ग्रामसभाओं को फर्जी तरीके से आयोजित कर अडानी समूह को कोयला खनन की स्वीकृति दी गई। ग्रामसभा की बैठक में जिन लोगों की उपस्थिति दिखाई गई, वे या तो गांव में रहते ही नहीं थे या उस दिन बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके खिलाफ कोयतुर समुदाय ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आदेश दिया। वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act) की धारा 3(1) में ट्राइबल जनजाति को सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार दिए गए हैं। वहीं धारा 4(5) कहती है कि अधिकार प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी को भी वनभूमि से हटाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही धारा 5 ग्रामसभा को यह अधिकार देती है कि वह अपने वन क्षेत्र की रक्षा करे, अतिक्रमण रोके और जैव विविधता की रक्षा करे। इसके बावजूद अनेक जिलों में बिना वन अधिकार की प्रक्रिया पूरी किए ही हजारों पेड़ काट दिए गए। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की परंपरा, संस्कृति और आत्मसम्मान का विनाश है।
न्यायपालिका की चेतावनी के बावजूद हो रहा है संविधान की अवहेलना
भारत के सर्वाेच्च न्यायालय ने कई बार इन अधिकारों की पुष्टि की है। 2013 में नियामगिरी जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रामसभा की सहमति के बिना खनन नहीं किया जा सकता। यह निर्णय ओडिशा के डोंगरिया कोंध आदिवासियों के पक्ष में था जिन्होंने अपनी पवित्र पहाड़ियों पर वेदांता कंपनी के खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अधिकार दिया कि वे तय करें कि वहां खनन होगा या नहीं। इसी तरह संपत मीणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामसभा को सर्वाेच्च निर्णयकर्ता माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने वन अधिकार मंच बनाम भारत सरकार केस में कहा कि बिना वन अधिकारों की पुष्टि के कोई परियोजना शुरू नहीं की जा सकती। ये सभी अदालती फैसलों के बावजूद सरकारें और कंपनियां संविधान, कानून और मानवता के खिलाफ जाकर कार्य कर रही हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और सरगुजा के गांवों में ग्रामसभा केवल नाम मात्र की रह गई है। वहां निर्णय पहले दिल्ली या रायपुर में लिया जाता है और फिर गांव में केवल उस निर्णय पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जो अक्सर झूठे दस्तावेजों के आधार पर होता है।
कोयतुर समुदाय से सीखें प्रकृति के साथ जीने की जीवनशैली
सरकार विकास के नाम पर “हरियर छत्तीसगढ़”, “गोधन न्याय योजना”, “वन धन योजना”, “नरवा गरवा घुरवा बाड़ी” जैसी योजनाएं चला रही हैं। परंतु इनका प्रभाव तभी होगा जब इनमें कोयतुर समुदाय की भागीदारी वास्तविक होगी। अभी ये योजनाएं अधिकतर ग्रीनवॉशिंग (हरित दिखावा) का उदाहरण हैं जहां रिपोर्ट में पर्यावरण बचाने की बात तो होती है पर ज़मीनी स्तर में जंगल उजाड़े का काम करते हैं। यह प्रकृति संरक्षण कोई अभियान नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है और यह दर्शन कोयतुर समुदाय से सीख सकते हैं। हमें विकास की परिभाषा को बदलना होगा। यदि विकास का मतलब जंगल काटना, नदियों को मोड़ना और जीवन को नष्ट करना है तो वह न विकास है न ही न्याय है, कोयतुर दर्शन हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही जीवन है और जब तक संतुलन रहेगा तब तक यह पृथ्वी बचे रहेगी।
सभी जनमानस जंगलों की चीख सुनें, उससे सीखें और दिशा बदलें
आइए इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लें कि हम केवल कानूनों को नहीं बल्कि संवेदनाओं को भी लागू करेंगे। हम प्रकृति को केवल संपत्ति नहीं, बल्कि संबंध मानेंगे। हम विकास को मुनाफे की नहीं, संतुलन की कसौटी को परखेंगे। जब तक कोयतुर समुदाय का जंगल बचेगा, तब तक धरती पर जीवन बचेगा। जंगलों के कटने का मतलब केवल पेड़ गिरना नहीं, एक पूरी सभ्यता का ढह जाना है। जब जंगल रोते हैं तो वह केवल हरियाली नहीं, मानवता की चीख होती है। हमें वह चीख सुननी होगी, उसे समझना होगा और उससे सीख लेकर एक नई दिशा की ओर बढ़ना होगा।
लेखक/विचारक: महेन्द्र सिंह मरपच्ची