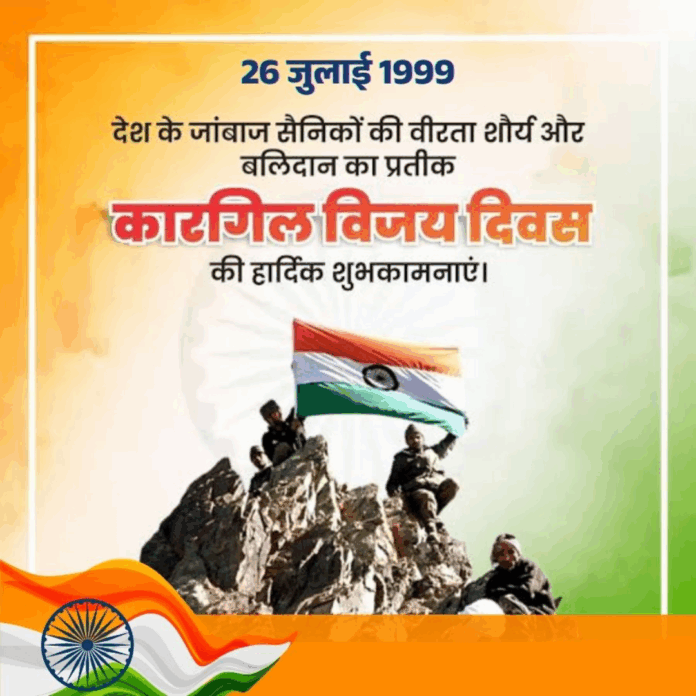26 जुलाई को भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व एक ऐसे युद्ध की स्मृति में नत होता है, जिसने मानवीय मूल्य, लोकतांत्रिक आदर्श और राष्ट्र की रक्षा के जज़्बे को सर्वोच्चता प्रदान की। यह दिन भारतीय सेना की अद्भुत वीरता का प्रतीक है, लेकिन इससे कहीं अधिक यह उस वैश्विक सन्देश का वाहक है जिसमें शांति के लिए शक्ति, मर्यादा के लिए संघर्ष और न्याय के लिए जागरूकता आवश्यक है। 1999 के कारगिल युद्ध को केवल एक सैन्य मुठभेड़ के रूप में देखना उस युद्ध की आत्मा से अन्याय होगा। यह संघर्ष था उस वैचारिक भिन्नता का जिसमें एक ओर भारत लोकतांत्रिक, मानवीय और न्यायपरक व्यवस्था के साथ खड़ा था और दूसरी ओर पाकिस्तान छद्म युद्ध, आतंकवाद और विश्वासघात की छाया में खेल रहा था।पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा कारगिल की ऊंची चोटियों पर घुसपैठ अंतरराष्ट्रीय कानून LOC की मर्यादा और द्विपक्षीय समझौतों का खुला उल्लंघन था। यह न केवल भारत की संप्रभुता के विरुद्ध था, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा और दक्षिण एशिया में शांति के भविष्य पर सीधा हमला था। भारत ने संयम, कूटनीति और निर्णायक सैन्य शक्ति का संतुलित प्रयोग करते हुए ‘ऑपरेशन विजय’ प्रारंभ किया और जून से जुलाई 1999 के बीच सभी रणनीतिक चोटियों को दुश्मन से मुक्त करा लिया। यह युद्ध उन 527 सैनिकों के बलिदान की अमरगाथा है जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस मातृभूमि की रक्षा में अर्पित की। कारगिल युद्ध की गूंज केवल हिमालय की पहाड़ियों तक सीमित नहीं रही। यह संघर्ष वैश्विक कूटनीति, सैन्य रणनीति और युद्ध नैतिकता की कसौटी बन गया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और संपूर्ण यूरोप ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। यह इतिहास में एक विरल क्षण था जब एक लोकतांत्रिक देश को बिना किसी पूर्व शर्त के अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि LOC का उल्लंघन वैश्विक शांति के लिए अस्वीकार्य है। यह युद्ध विश्व समुदाय को भी आइना दिखा गया। एक ओर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया, वहीं भारत ने Geneva Convention के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार किया, जिससे मानवीय गरिमा और युद्ध नैतिकता की एक नयी मिसाल बनी। इससे भारत की वैश्विक छवि और सुदृढ़ हुई। यह युद्ध उन राष्ट्रों के लिए चेतावनी बन गया जो आतंकवाद को नीति मानकर वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करना चाहते थे। कारगिल ने यह सिद्ध कर दिया कि छल से प्राप्त की गई ऊँचाइयाँ टिकती नहीं, और नैतिकता ही अंतिम विजय लाती है।
कारगिल युद्ध की गूंज केवल हिमालय की पहाड़ियों तक सीमित नहीं रही। यह संघर्ष वैश्विक कूटनीति, सैन्य रणनीति और युद्ध नैतिकता की कसौटी बन गया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और संपूर्ण यूरोप ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। यह इतिहास में एक विरल क्षण था जब एक लोकतांत्रिक देश को बिना किसी पूर्व शर्त के अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि LOC का उल्लंघन वैश्विक शांति के लिए अस्वीकार्य है। यह युद्ध विश्व समुदाय को भी आइना दिखा गया। एक ओर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया, वहीं भारत ने Geneva Convention के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार किया, जिससे मानवीय गरिमा और युद्ध नैतिकता की एक नयी मिसाल बनी। इससे भारत की वैश्विक छवि और सुदृढ़ हुई। यह युद्ध उन राष्ट्रों के लिए चेतावनी बन गया जो आतंकवाद को नीति मानकर वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करना चाहते थे। कारगिल ने यह सिद्ध कर दिया कि छल से प्राप्त की गई ऊँचाइयाँ टिकती नहीं, और नैतिकता ही अंतिम विजय लाती है।
कारगिल युद्ध शौर्य और संवेदना की अद्वितीय गाथा
इस युद्ध की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि भारत ने युद्ध को केवल सैन्य टकराव नहीं बनने दिया। यह एक नैतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध भी था। कारगिल में लड़ने वाले सैनिक केवल जवान नहीं थे, वे भारत की आत्मा के रक्षक थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की “यह दिल मांगे मोर” की गूंज, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव की अद्भुत बहादुरी, राइफलमैन संजय कुमार का अद्वितीय साहस और सैकड़ों अज्ञात सैनिकों का चुपचाप लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान, भारतीय जनमानस की चेतना में अमर हो गए। इन जवानों के पीछे खड़े थे उनके परिवार माँ, बहनें, पत्नियाँ और बच्चे जिन्होंने शोक को गर्व में बदला। यह एक ऐसा युग था जब पूरा राष्ट्र एक सैनिक परिवार में बदल गया था। महिलाओं ने न केवल अपनों को खोया, बल्कि देश को नया साहस भी दिया। भारत ने उस कठिन समय में न केवल अपने भीतर से शक्ति पाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि बलिदान केवल शोक नहीं, राष्ट्रनिर्माण की नींव भी होता है।
युद्ध के बाद की दुनिया: रणनीति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सम्मान
कारगिल विजय के बाद भारत की सुरक्षा नीति और कूटनीति दोनों ने एक नया मोड़ लिया। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना रक्षा क्षेत्र से ही सशक्त हुई। DRDO, HAL, ISRO और BEL जैसी संस्थाओं को युद्ध के अनुभवों से प्रेरणा लेकर स्वदेशी तकनीक के विकास का लक्ष्य मिला। रडार सिस्टम, ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और थल सेना के मॉडर्नाइजेशन को युद्ध के बाद तीव्र गति मिली। वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने अपनी परिपक्वता और शांतिप्रिय चरित्र को वैश्विक मंचों पर स्थापित किया। G20, BRICS, QUAD जैसी व्यवस्थाओं में भारत की भूमिका सशक्त हुई। कारगिल से यह संदेश गया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब सीमा, सम्मान और संप्रभुता पर हमला होता है, तो वह निर्णायक और नैतिक प्रतिरोध से पीछे नहीं हटता। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को मजबूती देने वाले राष्ट्र न केवल अपने लिए, बल्कि समूची मानवता के लिए खड़े होते हैं। कारगिल के बाद आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नीति में भी बदलाव आया। भारत की चेतावनी को अब अनसुना नहीं किया जाता, बल्कि उसे अनुभव का मार्गदर्शक माना जाता है।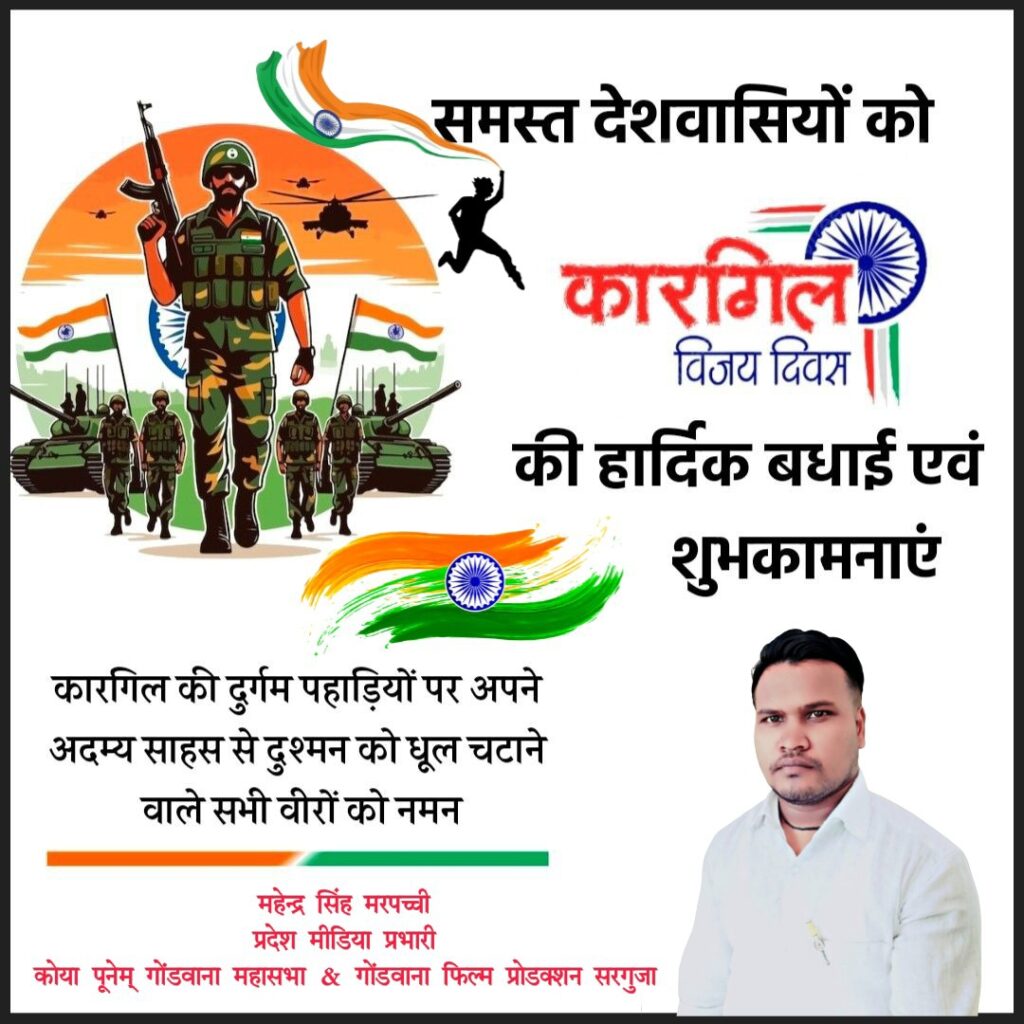 आज जब हम कारगिल विजय दिवस को विश्व स्तर पर स्मरण करते हैं, तो यह केवल सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिकता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझने का दिन भी है। कारगिल युद्ध में जो जज़्बा था—वह केवल सेना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह पूरे राष्ट्र का चरित्र बन गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज जो स्वतंत्रता, तकनीकी प्रगति, कूटनीतिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय स्वाभिमान हम अनुभव करते हैं, वह उस बलिदान की विरासत है जिसे कारगिल के रणबाँकों ने हमें सौंपा। इस विजय दिवस पर जब हम राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं, तो वह नमन केवल रंगों को नहीं, बल्कि उन मूल्यों को होता है जो उन रंगों से झलकते हैं—त्याग, साहस, और समर्पण। दुनिया के हर राष्ट्र को कारगिल जैसी घटनाओं से यह सीख लेनी चाहिए कि राष्ट्रों की शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक नहीं, नैतिक भी होनी चाहिए। तभी दुनिया एक ऐसी जगह बन सकती है, जहाँ सीमाएं न संघर्ष की रेखाएं हों, बल्कि सहअस्तित्व के पुल बनें। कारगिल विजय दिवस केवल भारत की जीत नहीं, यह मानवता की जीत है। यह युद्ध की विभीषिका में भी शांति की आशा ढूँढने का उदाहरण है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची विजय केवल भूमि पर नहीं, आत्मा में होती है। कारगिल हमें यह सिखाता है कि अगर लक्ष्य न्याय, राष्ट्र और मानवता है—तो हर युद्ध अनंत काल के लिए एक संदेश बन जाता है ।
आज जब हम कारगिल विजय दिवस को विश्व स्तर पर स्मरण करते हैं, तो यह केवल सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिकता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझने का दिन भी है। कारगिल युद्ध में जो जज़्बा था—वह केवल सेना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह पूरे राष्ट्र का चरित्र बन गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज जो स्वतंत्रता, तकनीकी प्रगति, कूटनीतिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय स्वाभिमान हम अनुभव करते हैं, वह उस बलिदान की विरासत है जिसे कारगिल के रणबाँकों ने हमें सौंपा। इस विजय दिवस पर जब हम राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं, तो वह नमन केवल रंगों को नहीं, बल्कि उन मूल्यों को होता है जो उन रंगों से झलकते हैं—त्याग, साहस, और समर्पण। दुनिया के हर राष्ट्र को कारगिल जैसी घटनाओं से यह सीख लेनी चाहिए कि राष्ट्रों की शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक नहीं, नैतिक भी होनी चाहिए। तभी दुनिया एक ऐसी जगह बन सकती है, जहाँ सीमाएं न संघर्ष की रेखाएं हों, बल्कि सहअस्तित्व के पुल बनें। कारगिल विजय दिवस केवल भारत की जीत नहीं, यह मानवता की जीत है। यह युद्ध की विभीषिका में भी शांति की आशा ढूँढने का उदाहरण है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची विजय केवल भूमि पर नहीं, आत्मा में होती है। कारगिल हमें यह सिखाता है कि अगर लक्ष्य न्याय, राष्ट्र और मानवता है—तो हर युद्ध अनंत काल के लिए एक संदेश बन जाता है ।